समाधि, पुरुष और ब्रह्मचर्य
चित्त की सम अवस्था को समाधि कहते हैं । समाधि से भिन्न अवस्था को मानसिक व्याधि कहते हैं । धारणा-ध्यान-समाधि में असमर्थ चञ्चल मन इतस्ततः विचरण करे तो विचार कहलाता है । विचार जब व्यवहार में उतरे तो आचार कहलाता है ।
पातञ्जल योग-सूत्र के अनुसार असम्प्रज्ञात समाधि से भिन्न अवस्था को "व्युत्थान" कहते हैं ('आत्मतत्व से योग की विपरीत दिशा में चित्त का उत्थान')। वास्तविक समाधि तो "असम्प्रज्ञात समाधि" है जिसमे चिन्तन भी संभव नहीं रहता, मन पूरा शांत और निष्क्रिय रहता है । लेकिन समाधि तो लग जाय और चित्त में प्रज्ञा कार्य करती रहे, तो उसे सम्प्रज्ञात समाधि (याज्ञवल्क्य की भाषा में "अमौन") कहते हैं । किन्तु सांसारिक व्यवहार में इन दोनों अवस्थाओं से बाहर निकलना पड़ता है । बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि भी समाधि में नित्य-कर्म नहीं कर सकते थे । तो क्या इसका यह अर्थ निकाला जाय कि नित्य-कर्म नहीं करना चाहिए ? कंप्यूटर आदि का प्रयोग यदि इन्द्रियोँ की तुष्टि के लिए किया जाय तो वह व्याधि है, वही कार्य यदि कर्तव्य और धर्म के उद्देश्य से किया जाय तो समाधि न रहते हुए भी योग के आठों अंगों के अंतर्गत ही माना जाएगा । जैसे की यम और नियम योग के अंग हैं लेकिन सांसारिक कार्यों के लिए हैं । जब उद्देश्य योग न रहे तब 'व्याधि' शब्द का प्रयोग करना उचित होगा ।
सारे विचार समाधि से भिन्न अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं । मन पूर्ण शान्त रहे तो चित्त में कोई भी वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होगी । विचार चित्त की वृत्ति है , किन्तु सारे विचार 'दोष' नहीं हैं ! सारी वृत्तियाँ भी दोष नहीं हैं । पहले तामसिक वृत्तियों से पिण्ड छुड़ाना पड़ता है , फिर राजसिक, और अन्त में सात्विक से भी ।
(वीर्यशुद्धि से स्मृति दृढ़ होती है |
स्मृति दृढ़ हो तो पहले पढ़ी हुई बातों का बाद में पढ़ी हुई बातों से तारतम्य बिठाना सहज हो जाता है | एक ही लेख में सारी बातों का समावेश सम्भव नहीं है | अतः जीवन में सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों, लेखों और अनुभवों को स्मृति में बनाए रखना चाहिए, तभी उन बातों का अर्थ समझ में आ सकता है जो किसी एक सन्दर्भ में स्पष्ट नहीं होती |
उदाहरणार्थ, हाल ही में एक टिपण्णी में मैंने लिखा की पुण्य का फल स्वर्ग होता है जिसके भोगने के बाद मर्त्यलोक में आना पड़ता है, और पाप का फल नरक होता है जिसके बाद फिर इसी मर्त्यलोक में ही आना पड़ता है | अतः पुण्य और पाप का अन्तिम लक्ष्य तो एक ही है -- मर्त्यलोक | पुण्य का फल है चार दिन की चाँदनी, और पाप का फल है चार अन्धेरी रातें | फिर उसके बाद ? तभी तो महाकवि विद्यापति ने लिखा - "माधव ! भव परिणाम निराशा !"
इस मर्त्यलोक से जो आशा रखते हैं वे कामनाओं के मायाजाल में बारम्बार फँसते हैं | संसार से निराशा ही (आत्म-) ज्ञान का द्वार खोलता है | सात्विक वृत्तियाँ भी चित्त की वृत्तियाँ ही हैं, और चित्त प्रकृति का अवयव है | जबतक प्रकृति से पुरुष का सम्बन्ध है तबतक जन्म-मरण का चक्र चलता रहेगा |
यही कारण है कि "पहले तामसिक वृत्तियों से पिण्ड छुड़ाना पड़ता है , फिर राजसिक, और अन्त में सात्विक से भी ।" इस क्रम को उलटाना मूर्खता है, पहले सात्विक से पिण्ड छुडायेंगे तो तामसिक वृत्तियाँ प्रभुत्व जमा लेंगी और सत्य की ओर प्रगति नहीं होने देंगी |)
शास्त्रानुकूल जो प्रेरणा दे, मूल प्रकृति की उस प्रधान विकृति को बुद्धि अथवा महत् कहते हैं । संकल्प करने की विकृति को मन कहते हैं । नयी सर्जना, अर्थात अपूर्व फल उत्पन्न करने को कल्प कहते हैं, जो यज्ञ का लक्ष्य होता है , अर्थात वास्तव में वस्तु को सर्जित करना 'कल्प' है । वास्तविकता से शून्य शाब्दिक ज्ञान को विकल्प कहते हैं, जो चित्त की पाँच प्रमुख वृत्तिओं में से एक है । चित्त की पाँच वृत्तियाँ हैं : प्रमाण (सही ज्ञान), विपर्यय (मिथ्या ज्ञान), विकल्प (वस्तुशून्य शाब्दिक ज्ञान), निद्रा ( अस्तित्व के अभाव की प्रतीति, अर्थात ज्ञान का अभाव), स्मृति (स्वयं के अनुभव की चित्त में पुनरावृति)। स्पष्ट है कि विकल्प और प्रमाण में भेद है । प्रमाण वास्तविक शब्दज्ञान है, विकल्प वस्तुशून्य शाब्दिक ज्ञान है । इन्हें ही 'विचार' कहते हैं । विचार प्रामाणिक हो तो सही हैं, अप्रामाणिक (विपर्यय या विकल्प पर आधारित) हो तो गलत हैं । लेकिन हर विचार वृत्ति ही है , जो चित्त का विकार है , विकृति है ।
चित्त की सभी वृत्तियाँ अनात्म के ज्ञान अथवा ज्ञान का अभाव है । चित्त जिस प्रकार के अनात्म-ज्ञान का साधन है, उसके ठीक विपरीत दिशा में योग की भूमियाँ हैं । सबसे ऊंची भूमि आत्मा का अपना स्तर है । उस स्तर पर व्यष्टि और समष्टि का, अपने और पराये का, दर्शक और दृश्य का, आत्म और अनात्म का, जीव और ईश्वर का, एवं जड़ और चेतन का भेद मिट जाता है, क्योंकि जहाँ तक जो कुछ भी है वह केवल "मैं" (आत्म) ही हूँ । यही कैवल्य है । सब कुछ मैं ही हूँ , तो शब्द और विचार का क्या प्रयोजन ? प्रमाण किस काम का ? आँख-नाक लेकर क्या करेंगे ? सब कुछ मैं ही हूँ तो शादी किससे करेंगे ? सब कुछ मैं ही हूँ तो इच्छा किस चीज की ? संकल्प किस बात का ? विकल्प किसलिए ? यही निर्विकल्पता है । सब कुछ मैं ही हूँ तो जानना किसे ? यही असम्प्रज्ञात है । स्वयं को जान लो, बस यही पर्याप्त है । किन्तु यह आसान नहीं ।
फल की इच्छा से रहित कर्तव्य कर्म संसार में अनिवार्य हैं, योग में बाधक नहीं हैं । सब कुछ मैं ही हूँ , इसका अर्थ यह नहीं कि माता और पत्नी में अन्तर नहीं । आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है , किन्तु लौकिक सम्बन्धों में लौकिक व्यवहार तब तक रखना ही पडेगा जब तक संसारचक्र से पूरी तरह मुक्ति न मिल जाय । आत्मज्ञान तर्क और विचार से नहीं मिलता । संस्कार भस्म करने पड़ते हैं ।
योग की पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ जानने के लिए गीताप्रेस का 'पातञ्जल योग प्रदीप' (स्वामी ओमानन्द तीर्थ) अच्छा ग्रन्थ है । संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों को अंग्रेजी माध्यम से सीखने के कारण ही आधुनिक युग में भारतीय दर्शन की दुर्दशा और विकृति हुई है । शिवराम वामन आप्टे का संस्कृत-हिन्दी शब्दकोष लें (संस्कृत-अंग्रेजी नहीं) और मूल धातुओं से शब्दों की निष्पत्ति स्वयं करके मूल अर्थ जानने प्रयास करें । कलियुग की लौकिक संस्कृत के अर्थ देवभाषा के मूल अर्थों पर थोपने से ऋषियों का ज्ञान समझ में नहीं आएगा । उदाहरणार्थ, निद्रा का मूल अर्थ है 'नीचे देखना' । लौकिक संस्कृत के वैयाकरण भी यह अर्थ नहीं मानेंगे क्योंकि आधुनिक डॉक्टरों की भाँति उन्हें निद्रा पसन्द है, जबकि योग-सूत्र निद्रा को दोष मानता है । आजकल लोग गर्व से अपने-आप को "सम्भ्रान्त" नागरिक कहते हैं, जबकि सम्भ्रान्त का अर्थ है 'सम्यक रूप से भ्रान्त' (पूर्ण पागल)। अतः देवभाषा के मूल दिव्य अर्थों को सावधानी पूर्वक जानने का प्रयास करना चाहिए । मानवों में वह सामर्थ्य नहीं जो ऐसी दिव्य भाषा बना सके ।
(उपरोक्त आलेख का पहला परिच्छेद चार वर्ष पहले का है, और शेष लेख उसी पुराने पोस्ट के नीचे की टिप्पणियाँ हैं जो बहुत कम लोग पढ़ पाए थे |)
*********************
डॉ.कृपाशंकर पाण्डेय जी ने प्रश्न उठाया है :--
<<<
साँख्ययोग की परम्परा पुरुषबहुत्व को स्वीकारती है तथा अद्वैत वेदान्त में अद्वयतत्त्व प्रधान है , ऐसी स्थिति में दोनों की मुक्ति में क्या अन्तर है..?
ईश्वरकृष्ण की साँख्यकारिका की कारिका संख्या 18 :
जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च ।
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव ।।
>>>
उत्तर :--
वेदान्त के अनुसार मुक्ति एक ही प्रकार की नहीं होती है और सभी प्रकारों को वेदान्त ने स्वीकृति दी है, किन्तु उसे "पुरुषबहुत्व" किस आधार पर कहा जा सकता है ? अद्वैत का यह अर्थ है कि मुक्त पुरुष का अस्तित्व मिट जाता है यह कहाँ लिखा है ? मोक्ष का अर्थ आत्मनाश वा आत्महत्या है ? अस्तित्व नहीं रहता तो वह "पुरुष" से एकीकृत न रहकर पृथक सत्ता बनाता है इसका क्या प्रमाण है ? राधाकृष्णन या हिरियन्ना जैसे लोगों को उद्धृत मत करें, जिनकी रूचि साँख्ययोग और समाधि में नहीं हैं उनको प्रमाणिक बताकर आप विषविद्यालय से डिग्री तो ले सकते हैं, किन्तु तब सात जन्मों तक साँख्ययोग में प्रवेश ईश्वर नहीं लेने देंगे, और इस बात का आपको पछतावा भी नहीं होगा | समाधि का अर्थ समझ जायेंगे तो ऐसे सारे प्रश्नों का अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा, यह प्रैक्टिकल से होता है , बहस से नहीं | असम्प्रज्ञात समाधि अद्वैत की अवस्था है, भले ही भिन्न-भिन्न लोग उस अवस्था में एक ही काल में हों और उनके भिन्न-भिन्न शरीर हों |
ईश्वरकृष्ण सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कब से हो गए ? साँख्यकारिका मूल ग्रन्थ नहीं, एक भाष्य है | उस भाष्य को भी समग्रता से समझने का प्रयास करेंगे तो उत्तम ग्रन्थ है, समग्र से काटकर लालबुझक्कड़ वाला अर्थ निकालेंगे तो गलत अर्थ मिलेगा | उसी में पढ़ें, चेतनत तत्व को "ज्ञ" कहा गया है, शेष सारे तत्व मूल प्रकृति के अंग हैं | "ज्ञ" एक है या बहुत ? पृथक ईश्वर की चर्चा नहीं है, जिस कारण बहुत से पढ़े लिखे मूर्खों ने सांख्य को नास्तिक कह दिया है | समाधि की अवस्था में जीवों और ईश्वर में पृथकता नहीं रहती, समाधि समत्व की एकल अवस्था है, अतः ज्ञान की अवस्था में केवल एक "ज्ञ" का ही अस्तित्व है | अज्ञान की अवस्था में जीवों में बहुत्व रहता है | उन जीवों में भी प्रकृति और पुरुष का भेद रहता है, आपके द्वारा उद्धृत अंश का यह तात्पर्य है | किन्तु यह अज्ञान की अवस्था है | पुरुष जब अज्ञान में है और बहुलता के भ्रम में है उसे सत्य मानेंगे या जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाय और अपने सच्चे "ज्ञ" अवस्था को पा ले उसे सत्य मानेंगे ? योग तो स्पष्ट तौर पर "स्वरुप" में अवस्थित होने का आदेश देता है, उसी को समाधि कहते हैं | वेदान्त के अनुसार मुक्त पुरुषों की मर्त्यलोक त्यागने के बाद भी कई प्रकार की अवस्थाएं संभव हैं, जिनमें एक सम्भावना यह भी है कि देवताओं और ऋषियों की तरह वे स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है की वे अलग-अलग पुरुष हैं | पुरुष का अर्थ है चैतन्यता | म्लेच्छों वाला मेल-फीमेल अर्थ सांख्ययोग पर थोपेंगे तो भूसा हाथ आयेगा | मुक्ति की तीन अवस्थाएं है - केवल मैं हूँ (मैं और ब्रह्म में अन्तर नहीं), मैं हूँ ही नहीं और सबकुछ "वह" है, और सिन्धुरूपी समष्टि में मैं एक "बिन्दु" है | बिन्दु अनेक हैं, किन्तु यह पुरुष की अनेकता नहीं है क्योंकि एक ही चैतन्यता सर्वत्र व्याप्त है | अनेकता माया है, भ्रम और अविद्या है | आपके प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा उद्धृत कारिका में ही है -- त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव | यह पुरुष का नहीं, प्रकृति का लक्षण है और प्रकृति से संगत के कारण पुरुष की अविद्या है |
अविद्या ही पुरुष में बहुत्व की भ्रामक माया का आभास कराता है | अविद्या असत है, इसका अस्तित्व वास्तव में है ही नहीं | एक ही पुरुष सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष है, सहस्रों जीवों में आत्मरूपी होकर विद्यमान है | उसके बिना किसी की सत्ता संभव ही नहीं है | आत्म का परम वही परमात्म तत्त्व है |
आर्यावर्त का प्रमुख वेद है शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा, जिसका अन्तिम यजु: कहता है कि "जो पुरुष आदित्य में है वही पुरुष मैं हूँ" | वेद का यह अन्तिम मन्त्र ही अद्वैत वेदान्त का आधार है | म्लेच्छों और उनके अनुचरों द्वारा स्थापित विषविद्यालय ऐसी बातों को विकृत करके गलत चीजें पढ़ाते हैं, जिनमें संस्कृत के वेतनभोगी प्राध्यापक भी पीछे नहीं हैं | शास्त्रीय परम्परा में वेद ही अन्तिम प्रमाण है, और वेद का दर्शन अद्वैत ब्रह्मवाद है |
"पुरुष" का अर्थ शारीरिक लिंगभेद से मत निकालें | पुरुष का अर्थ है विशुद्ध चैतन्यता, पुण्य का पुंसत्व | इसमें बहुत्व तभी सम्भव है जब कई प्रकार के सत्य, कई प्रकार के विशुद्ध चैतन्यता हों, किन्तु सत्य तो एक ही हो सकता है, कई सत्य होने की कल्पना ही असत्य है | अतः पुरुष एक ही हो सकता है | एक ब्रह्म ही अनेक बनता है यह ऋग्वेद का वचन है, जिसका अर्थ यह है की जीवों को भोग और मोक्ष का अवसर प्रदान करने के लिए एक ही पुरुष अनेक जीवों में अपने को स्थापित करता है और उनमें अपनी प्रकृति को भी स्थापित करता है ताकि वे सारे जीव अपने पिछले कर्मों का फल पायें और नए कर्म करें | किन्तु पुरुष का विखण्डन नहीं होता, जीवों की अनेकता उनकी प्रकृति की अनेकता है, उनके भौतिक शरीरों और अहंकार-जनित मिथ्या आत्मबोध की अनेकता है जो प्रकृति के अंग हैं, पुरुष के नहीं |
"विषविद्यालयीय गुरुओं" के पास सांख्ययोग जैसे विषयों में छात्र बनकर भी प्रवेश पाने की अर्हता नहीं होती क्योंकि उनको डिग्री आदि सांसारिक खिलौनों का लोभ है, वास्तविक ज्ञान की चाहत नहीं है | गीता में विष्णु भगवान् के पूर्णावतार श्रीकृष्ण ने स्वयं जिस "सांख्य" को ज्ञान की पराकाष्ठा कहा, उस दर्शन को विषविद्यालयीय गुरुओं ने केवल इस आधार पर नास्तिक ठहराया चूंकि उसमें जीव और ईश्वर का द्वैत नहीं है !! द्वैत नहीं है तो सांख्य अद्वैत हुआ न !! किन्तु ज्ञान की पराकाष्ठा पर सीधे नहीं पँहुचा जा सकता, सांख्य को समझने का एकमात्र उपाय है योग जिसे गीता में श्रीकृष्ण ने बल की पराकाष्ठा कहा | सांख्य के ज्ञान को जन्म-जन्मान्तरों की अविद्या ने बाधित कर रखा है जिसे योग का बल ही ध्वस्त कर सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है |
*********************
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी जीवों की ये तीन सामान्य अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति में आत्मज्ञान बना रहे उसी को तुरीयावस्था अर्थाय चौथी अवस्था कहते हैं जो समाधि का पर्याय है | व्याकरण के अनुसार तुरीय का अर्थ है चौथा, चत्वार भी च और त्वार का संयोग है जो तुरीय के धातु से ही बना है, जिसका सामान्य अर्थ है गतिशील होना, जड़ता त्यागना | जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति जड़ता की अवस्थाएं हैं, तुरीयावस्था में ही जड़ता से मुक्ति मिलती है, जीव चैतन्य बनता है |
जाग्रत मूर्खता की अवस्था है | स्वप्न में शरीर को आत्म मानकर उछल-कूद करते हैं, स्वप्न में चेतना बनी रहे इसके दीर्घ अभ्यास के बाद ही तुरीय मार्ग खुलता है | इसपर विस्तार से लिख चुका हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है |
*********************
सुषुप्तावस्था में हरेक प्राणी ब्रह्मलोक में रहता है और पिछले दिन की थकावट आदि नष्ट करके नयी जीवनी लेकर आता है | किन्तु जीवों का पाप उन्हें चेतन होकर ब्रह्मलोक का अनंत आनन्द भोगने का अधिकार नहीं देता, अतः अचेत होकर जीव सुषुप्तावस्था में ब्रह्मलोक गमन करते हैं | बिना सुषुप्तावस्था के कोई जीव जीवित ही नहीं रह सकता | किन्तु योगी चैतन्य होकर उसी अवस्था में रहता है, हालांकि अन्य लोगों के लिए उस काल में भी योगी सुषुप्तावस्था में ही डूबा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि योगी की इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार पूर्णतया सोये रहते हैं, किन्तु उसका जीव आत्मज्ञान को नहीं भूलता | इसी को योगनिद्रा कहते हैं |
पिछले लेखों को लोग याद नहीं रखते, अतः बातों को दुहराने के लिए कहते रहते हैं | बहुत पहले ही लिख चुका हूँ क इन्द्रियाँ जागी रहें तो जीव की उस अवस्था को "जाग्रति" कहते हैं |
इन्दियाँ सो जायँ किन्तु मन जागा रहे और अपने कार्य में लगा रहे तो उसे स्वप्न कहते हैं | मन का कार्य है संकल्प |
मन भी सो जाय तो उसे सुषुप्ति कहते हैं |
सामान्य जीव चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही ज्ञान रखता है | जब चित्त सो जाय तो कोई वृत्ति नहीं रहती, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है | किन्तु यह योग नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान से शून्य जीव तब सोचता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि चित्त के परदे पर जीव को कुछ नहीं दिखता |
किन्तु उसी सुषुप्ति में यदि जीव को आत्मबोध बना रहे तो इसे समाधि कहते हैं, तब जीव पूरे होश में रहता है और बुद्धि-अहंकार-मन सहित सारी इन्द्रियाँ सोयी रहती हैं | समाधि के गुण जब प्रभावी बन जाय तो मरणोपरान्त उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात प्रकृति से सम्बन्ध टूट जाता है, प्रकृति के अवयवों जैसे कि बुद्धि-अहंकार-मन सहित सारी इन्द्रियाँ से उसका सदा के लिए विच्छेद हो जाता है और विशुद्ध आत्मा के रूप में वह मुक्त हो जाता है |
मुक्ति के बाद भी यदि वह मुक्तपुरुष चाहे तो निर्माण-काया बनाकर मर्त्यलोक में आ सकता है, ऋषि ऐसे ही आते हैं | मृत्यु से पहले भी योगियों में निर्माण-काया बनाकर यत्र-तत्र गमन करने की शक्ति होती है | ऋषियों के संकल्प सत्य होते हैं, वे चाहे तो ब्रह्मा जी की तरह नयी-नयी सृष्टियाँ बना सकते हैं | किन्तु ब्रह्मा जी के कार्यों में दखलन्दाजी करने की भूल वे कर ही नहीं सकते |
*********************
मोक्ष किसी बोध का नहीं, बल्कि सच्चे आनन्द की अवस्था का नाम है, सप्तकोशों में उच्चतम कोश का नाम आनन्दमय कोश है जिसे ब्रह्मानन्द भी कहा जाता है | आत्मबोध के बाद आनन्द का पथ खुलता है |
आत्मबोध बिना गुरु के असम्भव है | किन्तु गुरु अपने मन से नहीं ढूंढना चाहिए | योग के मार्ग पर चलते रहने से समय आने पर ईश्वर गुरु से मिला देते हैं |
समाधि विशुद्ध आनन्द की अवस्था है, आत्मा की अपनी स्वाभाविक अवस्था है | जबकि ऐन्द्रिक आनन्द वास्तव में आनन्द नहीं हैं, वे तो केवल इन्द्रियों का अपने विषयों की ओर आकर्षण है जिसका इन्द्रियों को लाखों योनियों में बारम्बार जन्मों से अभ्यास बना हुआ है | यह आकर्षण भी अनवरत नहीं रहता, इन्द्रियों की तुष्टि होने पर ऐन्द्रिक आनन्द नष्ट हो जाता है | अतः इसे आनन्द कहना भ्रम है, माया है | ऐन्द्रिक भोग से जो तुष्टि मिलती है वह इन्द्रियों और मन की जड़ तुष्टि है जिसे अविद्या के लम्बे अभ्यास के कारण जीव आनन्द समझ लेता है | आत्मा के चैतन्य आनन्द का उसे अनुभव नहीं, अनुभव हो जाय तो ऐन्द्रिक तुष्टियों से जीव को वितृष्णा होने लगती है | इसी वैराग्य के अभ्यास को सतत बढाते रहना चाहिए | चित्त जड़ है, अभ्यास का गुलाम है | इसे ऐन्द्रिक भोग का अभ्यास है जिसे योग के दीर्घ अभ्यास से ही सुधारा जा सकता है |
अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक |
जो अहंकार दूसरों को दुःख देने में ही आनन्द का अनुभव करे और स्वयं को धर्म से विमुख करे वह तामसिक है | तामसिक अहंकार अन्ततः पतन कराता है |
जो अहंकार सांसारिक सुखों की ओर उन्मुख कराये वह राजसिक है |
जो अहंकार धर्म की ओर ले जाय वह सात्विक है |
इन्हें क्रमश: त्यागना चाहिए, अन्त में सात्विक अहंकार को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती -- आपकी अस्मिता यदि अहंकार में स्थित है तो आपकी अस्मिता वास्तविक आत्मा में स्थित नहीं हो सकती | अस्मिता कहते हैं "मैं" के भाव को |
सात्विक अहंकार भी जब नष्ट हो जाता है तो समाधि लगती है, तब आत्मा और परमात्मा का भेद मिटने लगता है | समाधि की आरम्भिक अवस्था में जीव को बोध रहता है, अपना भी और संसार का भी, जिसे सम्प्रज्ञात समाधि अथवा अमौन (शाब्दिक ज्ञान और चिन्तन) कहते हैं | इसमें सभी लोकों के तीनों कालों का ज्ञान योगी इच्छानुसार पा सकता है | सम्प्रज्ञात समाधि में ज्ञाता और ज्ञान का भेद रहता है, प्रज्ञा कार्य करती है | किन्तु यह वास्तविक समाधि नहीं है, केवल उसका आरम्भ है |
समाधि की वास्तविक अवस्था "असम्प्रज्ञात समाधि" अथवा मौन है, तब शब्दों में चिन्तन समाप्त हो जाता है, ऐसे मौन योगी को मुनि कहते हैं | चित्त में विचार का अन्त हो जाता है, कोई भी वृत्ति नहीं बचती | केवल आत्मतत्व का अपना अनुभव बचता है, और तब वह आत्मतत्व सर्वत्र सभी लोकों और सभी कालों में व्याप्त रहता है क्योंकि विशुद्ध चैतन्य को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, व्यक्ति और परमात्मा में भेद नहीं रहता, ज्ञाता और ज्ञेय में अन्तर नहीं रहता, क्योंकि सृष्टि भी आत्मतत्व के ब्रह्मा-रूप की केवल कल्पना है, अतः सबकुछ आत्म ही है | जब सबकुछ "मैं" ही हूँ तो जानने वाला और जानने की वस्तु में भेद नहीं रहता, केवल एक अद्वैत तत्व बचता है, इस सत्य अवस्था से पहले की सारी अवस्थाएं माया हैं, असत हैं | एक "मैं" के सिवा ब्रह्माण्ड में और कुछ भी नहीं है | इस "मैं" को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि "मैं" के सिवा कुछ है ही नहीं तो चाहा किसे जाय ? और जब चाहत ही नहीं, तो जन्म क्यों लें ?
ऐसा मुक्त पुरुष यदि चाहे तो जन्म ले सकता है किन्तु ऋषि की तरह केवल लोक-कल्याण के लिए, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं | ब्रह्मा जी केवल सृष्टि बनाते हैं, प्रजा की उत्पत्ति तो ऋषियों को आकर करना पड़ता है | वे ही सभी गोत्रों के प्रवर्तक हैं |
किन्तु हर मुक्त पुरुष ऋषि नहीं बन सकते | वैदिक मन्त्र-दृष्टा को ऋषि कहते हैं | विशिष्ट सिद्धियों के विशेषज्ञ को "सिद्ध" कहते हैं | ऐसे कई प्रकार के मुक्त पुरुष हैं | यहाँ "पुरुष" केवल आत्मा का बोध कराता है, इसमें नारी-शक्तियाँ भी आतीं हैं | देवता भी दो प्रकार के होती हैं, सूर्य-चन्द्र की तरह आजान देव जो अमर होते हैं और इन्द्रादि की तरह कर्मदेव जो कर्मों के कारण देवपद पाते हैं और मन्वन्तर समाप्त होते ही इन्द्रपद में दूसरा जीव आ जाता है |
*********************
ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म को प्राप्त करने वाला आचरण | वीर्य का अर्थ है जीव की आत्मा | जीवात्मा के मन में कामवासना घनीभूत होने पर वीर्य स्थूल रूप धारण करके नीचे गिरता है, यह आत्मा का पतन है | अतः वीर्यपात को आत्महत्या कहा जाता है | सनातन धर्म के गर्भाधान संस्कार के अनुसार सन्तान यज्ञ करने पर सन्तान भी उत्पन्न होता है और वीर्य का पतन भी नहीं होता | वासनामय वीर्य से वासना के कीड़े पैदा होते हैं जो कलियुग की कालिमा बढाते हैं |
पूरे कारण-शरीर को ही चित्त भी कहते हैं, किन्तु जबतक जीव स्थूल शरीर से जुड़ा है अर्थात जीवित है तबतक उसे चित्त कहते हैं, देहत्याग करने के बाद उसी चित्त को कारण-शरीर कहते हैं क्योंकि वह पृथक अस्तित्व बना लेता है | (इस उत्तर को कहीं सहेज कर रखिये, किसी पुस्तक में इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिलेगा, आधुनिक लेखक तो और भी भ्रांतियाँ फैलाते हैं |) मन उसका एक करण है |
Courtesy: https://www.facebook.com/100000039405456/posts/1911510155526946/
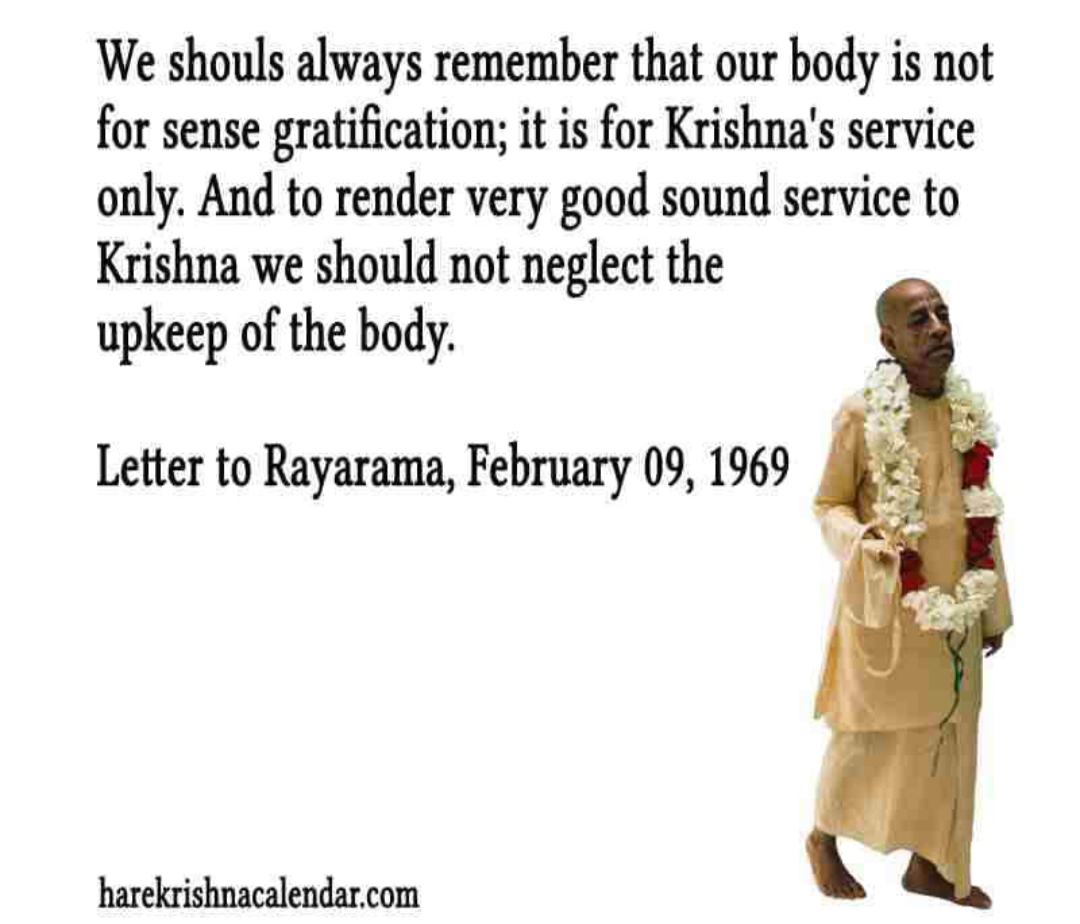
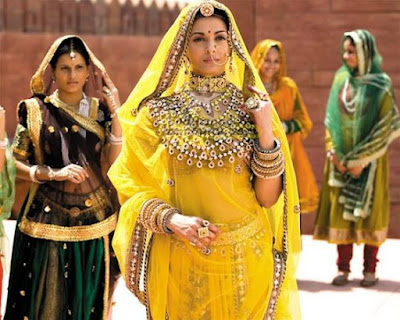





Comments
Post a Comment
कानूनों से फर्क पङता है. किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है जानना हो तो पता लगाओ की उस देश की न्याय प्रणाली कैसी है. देश में आर्थिक सामाजिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी न हो.
राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक-क्षमता में, अगर कोई देश अन्य देशों पर निर्भर रहता है तो उस देश का धर्म, न्याय, संस्कृति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व जनता तथा प्राकृतिक संसाधन कुछ भी सुरक्षित नहीं रह जाता.
वही राष्ट्र सेक्युलर होता है, जो अन्य देशों पर हर हाल में निर्भर हो.